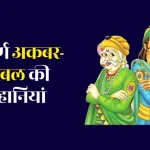Now Reading: श्रीमद् भागवत महापुराण (स्कन्ध 7) | Shrimad Bhagavatam Hindi
- 01
श्रीमद् भागवत महापुराण (स्कन्ध 7) | Shrimad Bhagavatam Hindi
श्रीमद् भागवत महापुराण (स्कन्ध 7) | Shrimad Bhagavatam Hindi
अध्याय 13: सिद्ध पुरुष का आचरण
संक्षेप विवरण: इस तेरहवें अध्याय में संन्यासियों के लिए अनुष्ठान दिये गये हैं और अवधूत के इतिहास का वर्णन भी हुआ है। इसकी समाप्ति विद्यार्थी के पूर्ण आध्यात्मिक उन्नयन के…
श्लोक 1: श्री नारद मुनि ने कहा : जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है उसे सारे भौतिक सम्बन्धों का परित्याग कर देना चाहिए और शरीर को सक्षम बनाये रखकर उसे प्रत्येक गाँव में केवल एक रात बिताते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार संन्यासी को शरीर की आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर रहे बिना सारे संसार में विचरण करना चाहिए।
श्लोक 2: संन्यास आश्रम के व्यक्ति को अपना शरीर ढकने के लिए वस्त्र तक का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि उसे कुछ पहनना हो तो उसे कौपीन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पहनना चाहिए और यदि आवश्यकता न हो तो संन्यासी को दण्ड भी नहीं धारण करना चाहिए। संन्यासी को दण्ड तथा कमण्डल के अतिरिक्त कुछ भी साथ में नहीं रखना चाहिए।
श्लोक 3: आत्मतुष्ट संन्यासी को चाहिए कि वह द्वार-द्वार से भीख माँगकर जीवन-यापन करे। किसी व्यक्ति या स्थान पर आश्रित न रहकर उसे समस्त जीवों का सुहृद् होना चाहिए। उसे नारायण का शान्त अनन्य भक्त होना चाहिए। इस प्रकार उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहना चाहिए।
श्लोक 4: संन्यासी को चाहिए कि वह परब्रह्म को प्रत्येक वस्तु में सदा व्याप्त देखने का प्रयास करे और ब्रह्माणु समेत प्रत्येक वस्तु को जिसमें यह ब्रह्माण्ड भी है, जो परब्रह्म पर टिका देखे।
श्लोक 5: उसे अचेतना तथा चेतना अवस्थाओं में इन दोनों के बीच की अवस्था में अपने आपको समझने का प्रयत्न करना चाहिए और आत्म-स्थित होना चाहिए। इस प्रकार उसे यह अनुभव करना चाहिए कि जीवन की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाएँ मात्र भ्रम हैं, वे वास्तविक नहीं हैं। ऐसे उच्च ज्ञान से उसे सर्वव्यापी परम सत्य का दर्शन करना चाहिए।
श्लोक 6: चूँकि भौतिक शरीर का विनाश निश्चित है और मनुष्य की आयु स्थिर नहीं है अतएव न तो मृत्यु की, न ही जीवन की प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रत्युत मनुष्य को नित्य काल का अवलोकन करना चाहिए जिसमें जीव अपने आपको प्रकट करता है और अन्तर्धान होता है।
श्लोक 7: समय का व्यर्थ अपव्यय कराने वाले अर्थात् आध्यात्मिक लाभ से विहीन साहित्य का तिरस्कार करना चाहिए। न तो कोई अपनी जीविका कमाने के लिए वृत्तिपरक शिक्षक बने, न वाद-विवाद में भाग ले। न ही वह किसी कारण या पक्ष की शरण ले।
श्लोक 8: संन्यासी को चाहिए कि वह न तो अनेक शिष्य एकत्र करने के लिए भौतिक लाभों का प्रलोभन दे, न व्यर्थ ही अनेक पुस्तकें पढ़े, न जीविका के साधन के रूप में व्याख्यान दे। न व्यर्थ ही भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने का कभी कोई प्रयास करे।
श्लोक 9: ऐसे शान्त समदर्शी व्यक्ति को जो आध्यात्मिक चेतना में सचमुच बढ़ा-चढ़ा है, संन्यासी के प्रतीकों—यथा त्रिदण्ड तथा कमण्डल—को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह आवश्यकतानुसार इन प्रतीकों को कभी धारण कर सकता है, तो कभी छोड़ सकता है।
श्लोक 10: साधु पुरुष भले ही मानव समाज के समक्ष अपने आपको प्रकट न करे, किन्तु उस के आचरण से उसका उद्देश्य प्रकट हो जाता है। उसे मानव समाज के समक्ष अपने को एक चंचल बालक की भाँति प्रस्तुत करना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ विचारवान् वक्ता होकर भी उसे अपने को मूक व्यक्ति की तरह प्रदर्शित करना चाहिए।
श्लोक 11: इसके ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में विद्वान मुनिजन एक प्राचीन वार्तालाप की कथा सुनाते हैं, जो प्रह्लाद महाराज तथा अजगर वृत्ति धारण किये एक महामुनि के मध्य हुआ था।
श्लोक 12-13: एकबार भगवान् के सर्वाधिक प्रिय सेवक प्रह्लाद महाराज अपने कतिपय विश्वस्त पार्षदों के साथ संत पुरुषों की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए विश्व का भ्रमण करने निकले। वे कावेरी तट पर पहुँचे जहाँ सह्य नामक एक पर्वत है। वहाँ पर उन्हें एक महान् साधु पुरुष मिला जो भूमि पर लेटा था और धूल-धूसरित था, किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से वह अत्यन्त बढ़ा-चढ़ा था।
श्लोक 14: लोग न तो उस साधु पुरुष के कर्मों से, न शारीरिक लक्षणों से, न उसके शब्दों से, न उसके वर्णाश्रम धर्म के लक्षणों से यह समझ पाये कि यह वही पुरुष है, जिसे वे जानते थे।
श्लोक 15: महाभागवत प्रह्लाद महाराज ने उस साधु पुरुष की विधिवत् पूजा की और प्रणाम किया जिसने अजगर-वृत्ति धारण कर रखी थी। इस प्रकार उस साधु पुरुष की पूजा करके तथा उसके चरणकमलों को अपने सिर से स्पर्श करके प्रह्लाद महाराज ने उसे समझने के उद्देश्य से विनीत भाव से इस प्रकार पूछा।
श्लोक 16-17: उस साधु पुरुष को अत्यन्त स्थूल (मोटा) देखकर प्रह्लाद महाराज ने कहा : महोदय, आप अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कोई उद्यम नहीं करते तो भी आपका शरीर उसी तरह हृष्ट पुष्ट है जैसाकि भौतिकतावादी कर्मी (भोगी) का होता है। मुझे ज्ञात है कि यदि कोई अत्यन्त धनी हो और उसके पास कुछ भी काम करने को नहीं हो तो वह खाकर, सोकर और कोई काम न करके अत्यधिक स्थूल (मोटा) हो जाता है।
श्लोक 18: हे अध्यात्मज्ञानी ब्राह्मण, आपको कुछ नहीं करना पड़ता जिसके कारण आप लेटे हुए हैं। यह भी माना जा सकता है कि इन्द्रियभोग के लिए आपके पास धन नहीं है। तो फिर आपका शरीर इतना स्थूल कैसे हो गया है? ऐसी परिस्थिति में यदि आप मेरे प्रश्न को प्रमादपूर्ण नहीं मानते तो कृपा करके बतलाएँ कि यह किस तरह से हुआ है?
श्लोक 19: आप विद्वान, दक्ष तथा सभी प्रकार से बुद्धिमान प्रतीत होते हैं। आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं और हृदय को भाने वाली बातें कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सामान्य लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं फिर भी आप यहाँ पर निष्क्रिय लेटे हैं।
श्लोक 20: नारद मुनि ने आगे कहा : जब दैत्यराज प्रह्लाद महाराज इस तरह से साधु पुरुष से प्रश्न कर रहे थे तो वह शब्दों की अमृत वर्षा से मुग्ध हो गया और उसने मुसकाते हुए प्रह्लाद महाराज की उत्सुकता का इस प्रकार जवाब दिया।
श्लोक 21: साधु ब्राह्मण ने कहा : हे असुरश्रेष्ठ, हे महान् तथा सभ्य पुरुष द्वारा सम्मान्य प्रह्लाद महाराज, आप जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से अवगत हैं, क्योंकि आप मनुष्य के चरित्र को अपनी स्वाभाविक दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं और इस तरह आप कर्मों की स्वीकृति तथा अस्वीकृति के परिणामों से भलीभाँति परिचित हैं।
श्लोक 22: भगवान् नारायण, जो समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं आपके हृदय में अग्रणी हैं क्योंकि आप शुद्ध भक्त हैं। वे सदैव अज्ञान के अंधकार को उसी तरह दूर करते हैं जिस प्रकार सूर्य ब्रह्माण्ड से अंधकार को दूर कर देता है।
श्लोक 23: हे राजन्, आप सब कुछ जानते हैं किन्तु आपने कुछ प्रश्न किये हैं, अतएव जैसा मैंने अधिकारियों से सुनकर सीखा है उसी के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। मैं इस मामले में मौन नहीं रह सकता, क्योंकि जो आत्मशुद्धि का इच्छुक है उसके द्वारा आप जैसे व्यक्ति से वार्तालाप करना उपयुक्त होगा।
श्लोक 24: अतृप्त भौतिक इच्छाओं के कारण मैं प्राकृतिक नियमों की तरंगों द्वारा बहा या लिए जा रहा था और जीवन की विभिन्न योनियों में जीवन-संघर्ष करते हुए विभिन्न कार्यकलापों में लगा रहा।
श्लोक 25: मैंने विकास प्रक्रिया के दौरान जो अवांछित भौतिक इन्द्रियतृप्ति के कारण सकाम कर्मों से उत्पन्न होती है यह मनुष्य रूप प्राप्त किया है, जो हमें स्वर्गलोकों तक, मुक्ति तक, निम्न योनियों तक या मनुष्य के बीच पुनर्जन्म लेने तक पहुँचा सकता है।
श्लोक 26: इस मनुष्य-जीवन में पुरुष तथा स्त्री का मिलन मैथुन-सुख के लिए होता है, किन्तु हमने वास्तविक अनुभव से देखा है कि उनमें से कोई भी सुखी नहीं है। इसीलिए विपरीत परिणामों को देखकर मैंने भौतिकतावादी कार्यों में भाग लेना बन्द कर दिया है।
श्लोक 27: जीवों के लिए जीवन का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक सुख का है और यही असली सुख है। यह सुख तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य सारे भौतिकतावादी कार्यकलापों को बन्द कर दे। भौतिक इन्द्रियभोग कोरी कल्पना है, अतएव इस विषय पर विचार कर मैंने सारे भौतिक कार्यकलाप बन्द कर दिये हैं और अब यहाँ लेटा हुआ हूँ।
श्लोक 28: इस प्रकार बद्ध आत्मा शरीर के भीतर रहकर अपने हित को भूल जाता है, क्योंकि वह अपनी पहचान शरीर के रूप में करने लगता है। चूँकि, शरीर भौतिक होता है अतएव उसकी सहज प्रवृत्ति भौतिक जगत की विविधताओं की ओर आकृष्ट होने की रहती है। इस तरह जीव इस संसार के कष्टों को भोगता है।
श्लोक 29: जिस प्रकार एक हिरन अज्ञानतावश घास से ढके कुएँ के जल को न देख कर जल के लिए अन्यत्र दौड़ता फिरता रहता है उसी प्रकार भौतिक शरीर से आवृत यह जीव अपने भीतर के सुख को नहीं देख पाता और भौतिक जगत में सुख के पीछे दौड़ता रहता है।
श्लोक 30: जीव सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख के कारणों से छूटना चाहता है, लेकिन चूँकी जीवों के शरीर प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं, अतएव जीव एक के बाद एक विभिन्न शरीरों को पाकर जितनी भी योजनाएँ बनाता है वे अन्ततोगत्वा व्यर्थ हो जाती हैं।
श्लोक 31: भौतिकतावादी कार्यकलाप सदैव तीन प्रकार के दुखों—अध्यात्मिक, अधिदैविक तथा अधिभौतिक—से मिले-जुले होते हैं। अतएव यदि कोई ऐसे कार्य सम्पन्न करके कुछ सफलता प्राप्त भी कर ले तो उससे क्या लाभ है? उसे फिर भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि तथा अपने कर्मफलों को भोगना होगा।
श्लोक 32: ब्राह्मण ने आगे कहा : मैं सचमुच देख रहा हूँ कि अपनी इन्द्रियों के वशीभूत हुआ एक धनी व्यक्ति किस तरह धन संचित करने का अत्यन्त लोभी होता है। अतएव सम्पत्ति तथा ऐश्वर्य होते हुए भी चारों ओर से भय के कारण वह अनिद्र रोग का शिकार बन जाता है।
श्लोक 33: जिन्हें भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली तथा धनी माना जाता है वे सामान्यत: सरकारी नियमों, चोर-उचक्कों, शत्रुओं, स्वजनों, पशुओं, पक्षियों, दान लेने वालों, काल, यहाँ तक कि अपने आप से चिन्तित रहते हैं। इस प्रकार वे अनिवार्यत: भयभीत रहते हैं।
श्लोक 34: मानव समाज के बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे शोक, लोभ, भय, क्रोध, अनुराग, दरिद्रता तथा अनावश्यक श्रम के मूल कारण को त्याग दें। इन सबों का मूल कारण अनावश्यक प्रतिष्ठा तथा धन की लालसा है।
श्लोक 35: मधुमक्खी तथा अजगर दो श्रेष्ठ गुरु हैं, जो हमें इस सम्बन्ध में आदर्श उपदेश देते हैं कि किस तरह थोड़ा-थोड़ा संग्रह करके सन्तुष्ट रहा जाये और किस तरह एक ही स्थान में ठरहा जाये—हिला न जाये।
श्लोक 36: मधुमक्खी से मैंने सीखा है कि धन संग्रह करने से किस तरह विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि यद्यपि धन शहद जैसा है, किन्तु कोई भी धन के स्वामी को मार कर धन को ले जा सकता है।
श्लोक 37: मैं किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करता, अपितु जो कुछ भी अपने आप मिल जाता है उसी से सन्तुष्ट रहता हूँ। यदि मुझे कुछ भी नहीं मिलता तो अजगर की तरह मैं अविक्षिप्त रहते हुए धैर्यपूर्ण रहता हूँ और कई-कई दिनों तक पड़ा रहता हूँ।
श्लोक 38: कभी मैं थोड़ा खाता हूँ और कभी अधिक। कभी भोजन स्वादिष्ट होता है, तो कभी बासी। कभी बड़े आदर के साथ मुझे प्रसाद दिया जाता है और कभी अत्यन्त उपेक्षा से भोजन मिलता है। कभी मैं दिन में खाता हूँ तो कभी रात में। इस प्रकार मुझे जो कुछ आसानी से मिल जाता है उसे ही खाता हूँ।
श्लोक 39: शरीर ढकने के लिए मेरे भाग्य से मुझे जो कुछ भी मिल जाता है, चाहे क्षौम वस्त्र हो या रेशमी या सूती कपड़ा, चाहे पेड़ की छाल हो या मृगछाला, उसे मैं काम में लाता हूँ। मैं पूर्ण संतुष्ट रहता हूँ तथा विचलित नहीं होता।
श्लोक 40: कभी मैं पृथ्वी पर, कभी पत्तियों पर, घास या पत्थर पर तो कभी राख के ढेर पर अथवा कभी-कभी अन्यों की इच्छा से महल के उच्च कोटि के बिस्तर तथा तकिये पर सोता हूँ।
श्लोक 41: हे स्वामी, कभी मैं ठीक से स्नान करके सारे शरीर में चन्दन का लेप करता हूँ, फूलों की माला पहनता हूँ और सुन्दर वस्त्र तथा आभूषण धारण करता हूँ। फिर मैं राजा की तरह हाथी की पीठ पर या रथ या घोड़े पर सवार होकर विचरण करता हूँ। किन्तु कभी-कभी मैं भूत-प्रेत द्वारा सताये व्यक्ति की तरह नंग-धड़ंग घूमता हूँ।
श्लोक 42: विभिन्न लोग विभिन्न स्वभाव के होते हैं; अतएव उनकी प्रशंसा करना या उनकी निन्दा करना मेरा कार्य नहीं है। मैं तो इस आशा से उनके कल्याण की कामना करता हूँ कि वे परमात्मा, भगवान् श्रीकृष्ण के साथ एकात्मता स्वीकार करेंगे।
श्लोक 43: अच्छे तथा बुरे के भेदभाव की जो मानसिक कल्पना (मनोरथ) है उसे इकाई रूप में स्वीकार करके उसे मन में लगाना चाहिए और तब मन को मिथ्या अहंकार में लगाना चाहिए। इस मिथ्या अहंकार को माया में लगाना चाहिए। मिथ्या भेदभाव से लडऩे की विधि यही है।
श्लोक 44: विद्वान विचारवान् व्यक्ति को इसकी अनुभूति होनी चाहिए कि यह भौतिक जगत मोह है किन्तु ऐसा आत्म-साक्षात्कार द्वारा ही सम्भव है। ऐसे स्वरूपसिद्ध व्यक्ति को, जिसने सत्य का वास्तविक साक्षात्कार किया है, आत्म-साक्षात्कार होने के कारण समस्त भौतिक कार्यकलापों से अवकाश ले लेना चाहिए।
श्लोक 45: प्रह्लाद महाराज, आप निश्चय ही स्वरूपसिद्ध आत्मा तथा भगवद्भक्त हैं। आप न तो जन-मत की परवाह करते हैं, न ही तथाकथित शास्त्रों की। इस कारण मैंने आपसे नि:संकोच भाव से अपने आत्म-साक्षात्कार का इतिहास कह सुनाया।
श्लोक 46: नारद मुनि ने आगे कहा : साधु से ये उपदेश सुन कर असुरराज प्रह्लाद महाराज पूर्ण पुरुष (परमहंस) के वृत्तिपरक कर्तव्य समझ गये। इस प्रकार उन्होंने उस सन्त की विधिपूर्वक पूजा की और उससे अनुमति लेकर अपने घर के लिए विदा हुए।